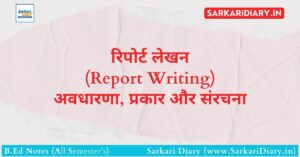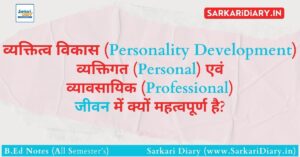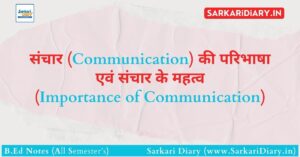भारत की सामाजिक प्रणाली में शक्ति व प्राधिकार की स्थिति
भारत की सामाजिक व्यवस्था का इतिहास प्राचीन काल से ही जटिल रहा है। वैदिक काल में परिवार के मुखिया पिता होते थे और स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था। स्त्रियों को देवतुल्य माना जाता था तथा शिक्षा भी सीमित रूप में प्रचलित थी। बौद्ध काल में भी स्त्रियों को शिक्षा का अवसर मिला।
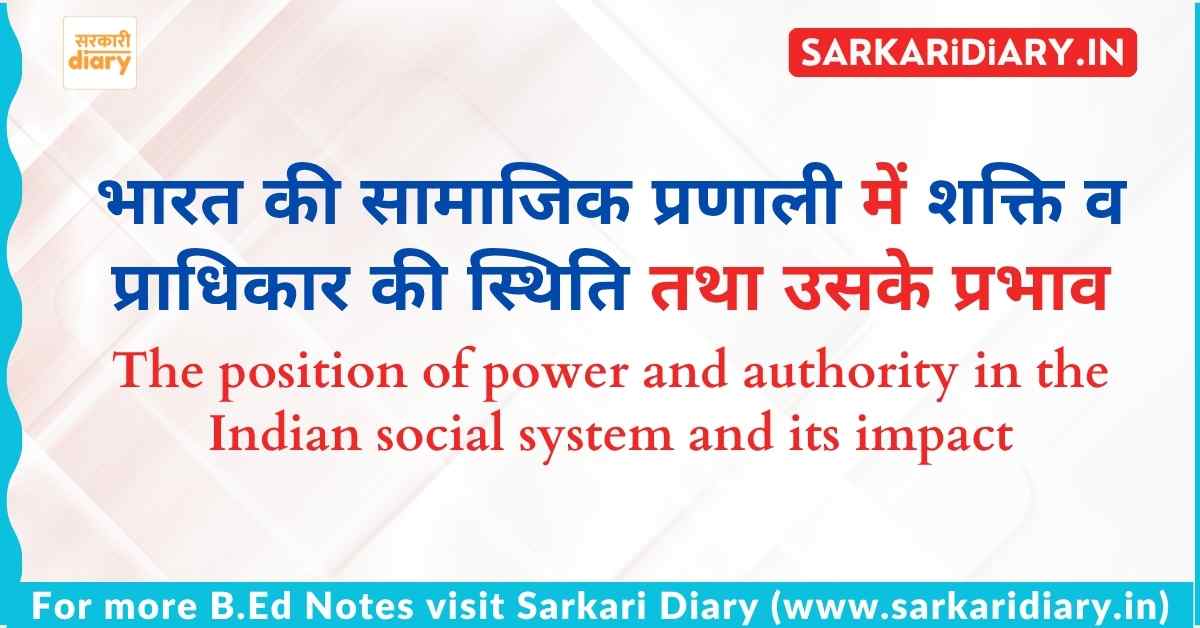
मध्ययुग में मुस्लिम आक्रमण और सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, दहेज, बालविवाह ने स्त्रियों की स्थिति कमजोर की। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। स्वतंत्रता के बाद संविधान ने समानता, अस्पृश्यता उन्मूलन और महिला शिक्षा के लिए नियम बनाए।
परंतु वर्तमान में भारतीय परिवार प्रायः पितृसत्तात्मक हैं, जहाँ पिता के पास परिवार में अधिक शक्ति व प्राधिकार होते हैं। विवाह के बाद स्त्रियाँ पति के परिवार की जाति, उपनाम अपनाती हैं। पिता का नाम ही बच्चों के प्रमाणपत्रों और अन्य दस्तावेजों में लिखा जाता है। अधिकांश संपत्ति का अधिकार भी पिता या पुरुष सदस्यों के पास होता है।
कुछ जनजातीय समाज जैसे खासी और गारो मातृसत्तात्मक हैं, जहां शक्ति स्त्रियों के पास होती है और वंश माँ से चलता है।
समाज में व्यापक पितृसत्ता के कारण बालकों को बालिकाओं की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण में भेदभाव रहता है। बालिकाओं को घरेलू कामों में व्यस्त रखा जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। बालिकाओं के विवाह जल्दी कर दिए जाते हैं और उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है।
हालांकि धीरे-धीरे समाज में परिवर्तन हो रहा है:
- लड़कियाँ शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं।
- सरकारी योजनाओं से बालिकाओं को शिक्षा में सहायता मिल रही है।
- स्त्रियों को कुछ अधिकार व सम्मान मिल रहे हैं।
शिक्षा हेतु विशिष्ट जेंडर प्रभाव
भारत में लड़कियों की शिक्षा में कई बाधाएं हैं, जैसे:
- जेंडर आधारित मानसिकता और परिवार में भेदभाव।
- बालिकाओं को घरेलू कार्यों में व्यस्त रखना।
- स्कूलों की दूरी और बालिकाओं की सुरक्षा की चिंता।
- बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियाँ।
- महिला शिक्षकों की कमी।
- बालिका विद्यालयों, छात्रावासों की अपर्याप्तता।
इन कारणों से लड़कियों का नामांकन कम होता है और वे पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं।
शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए अपेक्षित सामाजीकरण
सामाजीकरण का अर्थ है व्यक्ति को समाज की परंपराओं, मूल्यों, नियमों के अनुसार तैयार करना। जेंडर समानता के लिए सामाजीकरण में निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है:
- समाज में जेंडर आधारित भेदभाव को समाप्त करना।
- बालिकाओं को शिक्षा के लिए समान अवसर देना।
- परिवारों और समाज में लड़कियों की शिक्षा की आवश्यकता को स्वीकार करना।
- सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना ताकि अधिक बालिकाएँ लाभान्वित हों।
- बालिकाओं के लिए सुरक्षित और सुगम शिक्षा वातावरण सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं को घरेलू कार्यों से मुक्त कर पढ़ाई पर ध्यान देना।
- सामाजिक रूढ़ियों जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि का उन्मूलन।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष लक्ष्य तथा योजनाएं बनाई गईं हैं, जैसे-
- प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना।
- प्रौढ़ शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में महिलाओं के अवसर बढ़ाना।
- अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं विकलांग बालिकाओं के लिए विशेष योजनाएं।
- महिला शिक्षकों की भर्ती बढ़ाना।
निष्कर्ष
भारत की सामाजिक प्रणाली में शक्ति व प्राधिकार की स्थिति प्रायः पितृसत्तात्मक है जिससे महिलाओं व बालिकाओं की स्थिति द्वितीयक रहती है। शिक्षा में जेंडर आधारित भेदभाव समाज की एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा हेतु समान अवसर और जेंडर समानता प्राप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों में उचित सामाजीकरण और सरकारी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।
सामाजिक सोच में परिवर्तन, शिक्षा की समतामूलक व्यवस्था और बालिकाओं को सुरक्षित शिक्षा वातावरण उपलब्ध कराने से ही बालिकाओं का सशक्तिकरण संभव है। इससे समाज में लिंग आधारित भेदभाव समाप्त हो सकता है और समान अवसर मिल सकते हैं।