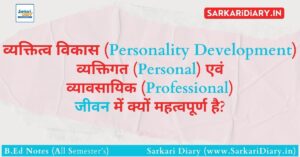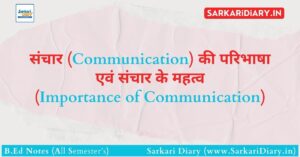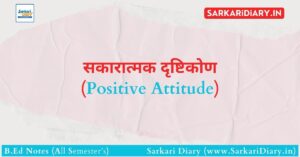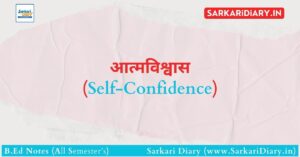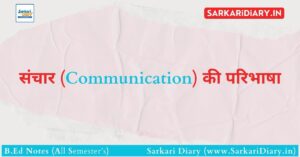भारत में बालिकाओं की शिक्षा की असमानता
भारत में बालिका शिक्षा का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षित महिला न केवल अपने परिवार को शिक्षित बनाती है बल्कि समाज के हर क्षेत्र में पुरुषों के समान, या कभी-कभी उनसे बेहतर प्रदर्शन भी करती है। शिक्षा प्राप्त महिला कुशल व्यवसायी, समाजसेवी, चिकित्सक, इंजीनियर, तकनीशियन या राजनेता बनकर राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे सकती है। शिक्षा से नारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है।
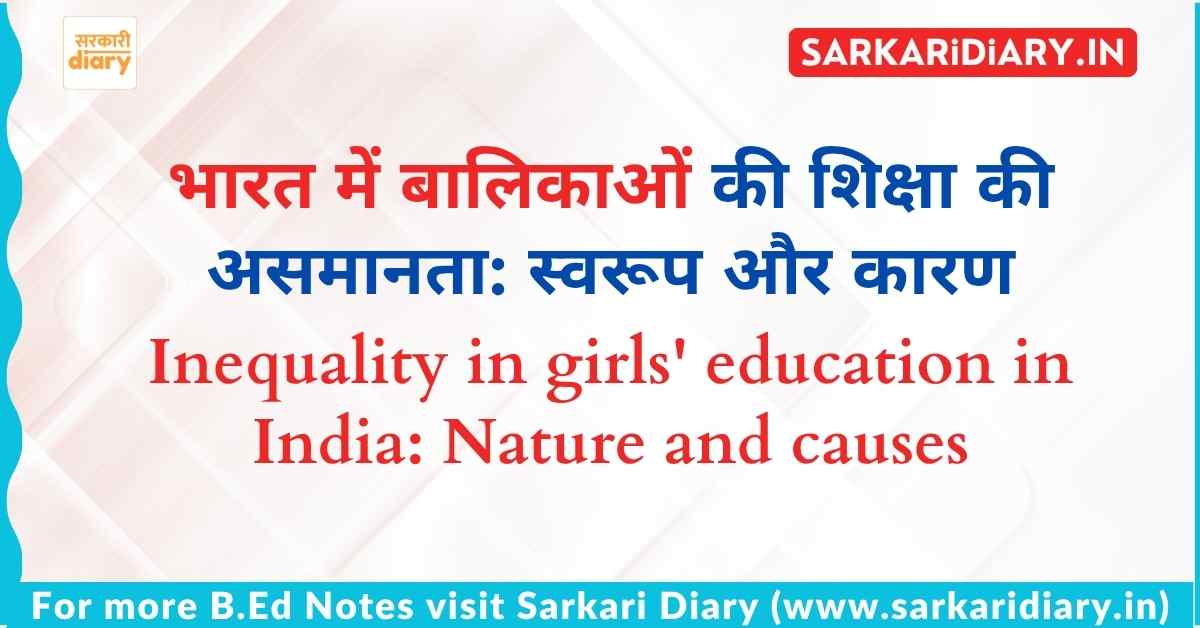
बालिका शिक्षा में असमानता के स्वरूप
भारतीय जनगणना के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है। उदाहरण के लिए, 2001 की जनगणना में पुरुषों की साक्षरता दर 75.85% थी जबकि महिलाओं की मात्र 54.16% थी। साक्षरता के इस अंतराल (लगभग 21.69%) को देखें तो यह 1951 से लेकर 1991 तक लगभग लगातार 18% से 26% के बीच रहा है, जो चिंताजनक है।
बालिकाओं के स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) की दर बहुत अधिक है, विशेष रूप से उच्च शिक्षा स्तर पर उनकी उपस्थिति और भी कम होती है। जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है, बालिकाओं की संख्या में गिरावट आना आम है।
बालिका शिक्षा में कमी के कारण
जनमानस की मानसिकता:
समाज में यह धारणा है कि लड़कियों को नौकरी या करियर बनाने की बजाय केवल घरेलू काम सिखाया जाए। इसलिए कई परिवार लड़कियों की शिक्षा को सीमित रखते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ाई करने वाली लड़की को अच्छा वर नहीं मिलेगा, या उसे अधिक दहेज देना पड़ेगा।
घरेलू कार्यों में व्यस्तता:
विशेषकर ग्रामीण और नगरीय गरीब इलाकों में लड़कियों को घरेलू काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, भाई-बहनों की देखभाल आदि में लगाया जाता है, जिससे पढ़ाई पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है।
पृथक विद्यालयों की कमी और दूरी:
लड़कियों के लिए अलग से स्कूल नहीं होना या स्कूलों का घर से दूर होना उनके पढ़ाई छोड़ने का एक बड़ा कारण है। कई अभिभावक लड़कियों को दूर भेजने से कतराते हैं, खासकर सह-शिक्षा वाले स्कूलों में।
कुप्रथाएं:
बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बुरका प्रथा जैसी सामाजिक प्रथाएं लड़कियों की शिक्षा के रास्ते में बाधा हैं। मुस्लिम और कुछ हिंदू समुदायों में यह प्रथाएं बालिका शिक्षा को प्रभावित करती हैं।
बालिका श्रम प्रथा:
गरीबी के कारण कई लड़कियां घरेलू या बाहरी कामों में व्यस्त रहती हैं, जिससे उनका विद्यालय जाना मुश्किल हो जाता है।
कानूनी व्यवस्था का सही क्रियान्वयन न होना:
2009 में लागू ‘बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम’ के बावजूद जमीन स्तर पर इसे सही ढंग से लागू नहीं किया जा सका है। कई बच्चे, खासकर लड़कियां, अभी भी स्कूल नहीं जातीं।
प्रोत्साहन योजनाओं का अभाव:
केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं जैसे साइकिल योजना, छात्रावास, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन योजना आदि, लेकिन बजट की कमी और प्रचार की कमी के कारण वे पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पा रही हैं।
सुरक्षा की समस्या:
कई जगह लड़कियों के स्कूल जाते समय छेड़छाड़ और असामाजिक तत्वों की समस्या होती है, जिससे परिवार उन्हें स्कूल भेजने में हिचकते हैं।
आर्थिक तंगी:
गरीब परिवार लड़कियों के शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर पाते, जिससे कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं या उच्च शिक्षा नहीं कर पातीं।
रोजगार की कमी:
पढ़ी-लिखी लड़कियों के लिए नौकरी के अवसर सीमित हैं, खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में। इसके कारण वे पढ़ाई में रुचि खो बैठती हैं।
पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री में कमी:
बालिकाओं के लिए विशेष रूप से स्त्री-संबंधित या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की कमी भी उनकी उच्च शिक्षा में बाधा है।
महिला शिक्षकों की कमी:
लड़कियों के विद्यालयों में महिला शिक्षकों की कमी भी पढ़ाई के लिए एक बाधा है।
उच्च शिक्षा के लिए दूरस्थ शिक्षा और छात्रावास सुविधाओं की कमी:
कई परिवारों में लड़कियों को दूर जाकर रहने की अनुमति नहीं मिलती, इसलिए वे उच्च शिक्षा नहीं कर पातीं।
इतिहास की झलक
वैदिक काल में बालिकाओं को सीमित शिक्षा घर पर दी जाती थी। कुछ विदुषी महिलाएं भी थीं जो वेदों में प्रवीण थीं। परन्तु बाल विवाह की प्रथा के कारण बालिकाओं की शिक्षा में बाधा आई। बौद्ध काल में कुछ हद तक सुधार हुआ, किन्तु सामान्य बालिकाएं शिक्षा से वंचित रहीं। मुस्लिम काल में पर्दा प्रथा और सामाजिक बंदिशों ने बालिका शिक्षा को और सीमित कर दिया। ब्रिटिश शासन में भी शिक्षा का दायरा मुख्यतः उच्च वर्ग तक सीमित रहा।
स्वतंत्रता के बाद की स्थिति
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं, आयोग और नीतियां बनाईं। संविधान में महिलाओं को समान अधिकार दिए गए। राधाकृष्णन आयोग, दुर्गाबाई देशमुख समिति, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आदि ने बालिका शिक्षा के लिए सुझाव और योजनाएं दीं। सरकारें छात्रवृत्ति, छात्रावास, साइकिल योजना, कस्तूरबा गांधी योजना जैसे कार्यक्रम चला रही हैं, जो बालिकाओं के नामांकन और पढ़ाई को प्रोत्साहित करते हैं।
निष्कर्ष
बालिका शिक्षा में असमानता के कई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारण हैं। इनसे निपटने के लिए जनमानस की सोच बदलना, स्कूलों की सुविधा बढ़ाना, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, कानूनों का कड़ाई से पालन करना और शिक्षा के लिए पर्याप्त बजट देना जरूरी है। तभी भारत में लड़कियों को शिक्षा का समान अवसर मिल सकेगा और वे देश के विकास में अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभा पाएंगी।