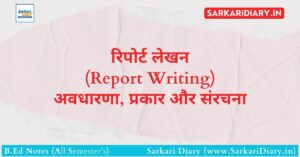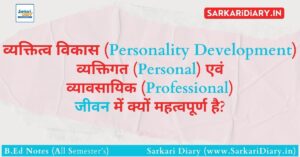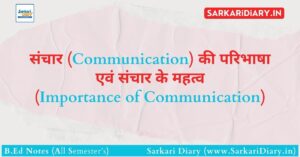समानता मानव स्वभाव का मूल अधिकार है। जन्म के समय सभी मनुष्य समान और स्वतंत्र होते हैं। प्राकृतिक रूप से पुरुष और महिला दोनों में शारीरिक और भावनात्मक भिन्नता हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनमें सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक समानता का भेद हो। इतिहास में देखा गया है कि महिलाएं ममता, करुणा, नैतिकता, धैर्य, क्षमा और दया की प्रतिमूर्ति मानी गईं, परन्तु फिर भी उन्हें अक्सर उपेक्षा, पीड़ा और सामाजिक अन्याय का सामना करना पड़ा। पुरुष समाज ने महिला को पराधीन बनाकर अपनी सत्ता को स्थायी करने का प्रयास किया, जिससे महिला का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थान कमजोर हुआ। महिला को अक्सर सांस्कृतिक और पारंपरिक सजावट के रूप में देखा गया, जबकि वास्तविक सामाजिक स्थिति में वह पुरुष की तुलना में द्वितीय श्रेणी की रही।

अव्यवस्थित आदिम युग में लैंगिक असमानता का उदय
मानव जाति के प्रारंभिक काल में नारी की स्थिति स्वतंत्र और सम्मानित थी। उस समय मातृसत्तात्मक समाज था, जहाँ संतान माता के नाम से जानी जाती थी। विवाह की एकनिष्ठ प्रथा नहीं थी और यौन संबंध अनियंत्रित थे। इस काल में नारी की सत्ता स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य थी।
समय के साथ जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ी, संपत्ति और उत्तराधिकार के प्रश्न उत्पन्न हुए, पुरुषों ने सामाजिक व्यवस्था को पितृसत्तात्मक बनाया। इसके कारण निम्न परिवर्तन हुए:
- विवाह में एकनिष्ठता का आरंभ
- परिवार और संपत्ति का पुरुषों द्वारा नियंत्रण
- नारी की स्थिति में गिरावट
- महिलाओं को केवल संतानोत्पत्ति और परिवार चलाने तक सीमित कर दिया गया
- नारी को पुरुष की दासी और संपत्ति का हिस्सा नहीं माना गया
इस संक्रमणकालीन दौर में नारी की सामाजिक प्रतिष्ठा कमजोर हुई और पुरुष सत्ता ने समाज पर पकड़ मजबूत की।
प्राचीन भारतीय संस्कृति में लैंगिक समानता और असमानता
(i) वैदिक काल में समानता
वैदिक समाज में महिलाओं को विशेष सम्मान प्राप्त था। कन्याओं को शिक्षा दी जाती थी, वे शास्त्रार्थ में भाग लेती थीं (जैसे विदूषी गार्गी का उदाहरण)। बालक और बालिका की शिक्षा में कोई भेद नहीं था। महिला स्वतंत्र वातावरण में रहती थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, और पुत्री के जन्म की निंदा नहीं की जाती थी।
(ii) मनुस्मृति में लैंगिक असमानता
मनुस्मृति में महिलाओं के अधिकारों पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। पुत्र को पुत्री से अधिक महत्व दिया गया, स्त्रियों को वेद अध्ययन से वंचित किया गया, पति को पत्नी का स्वामी माना गया। पत्नी को पतिव्रता रहना अनिवार्य था और असंतुष्टि पर उसे घर से निकालना भी उचित माना गया। महिलाओं को सार्वजनिक धार्मिक कार्यों से भी बाहर रखा गया।
(iii) कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लैंगिक असमानता
कौटिल्य ने महिलाओं को चंचल, अविश्वसनीय और अशुभ बताया। उन्हें पिता के घर जाने की स्वतंत्रता नहीं दी गई। पुत्रहीन विधवाओं को पति की संपत्ति से वंचित किया गया। महिलाओं को नियंत्रण में रखने की नीति अपनाई गई।
(iv) मध्यकालीन भारत में लैंगिक असमानता
मुगलकालीन दौर में महिलाओं की सामाजिक स्थिति और अधिक दयनीय हुई। बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, अशिक्षा, और अंधविश्वास ने महिलाओं को पराजित और उपेक्षित बनाया। हालांकि इस काल में कई महिलाओं ने स्वयं अपनी प्रतिभा और साहस का परिचय दिया, फिर भी व्यापक सामाजिक सुधार का अभाव रहा।
अंग्रेजों का आगमन एवं नवीन युग का सूत्रपात
अंग्रेजों के आगमन के बाद भारतीय समाज में महिलाओं की दशा में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ। विदेशी शासन ने सामाजिक सुधारों में हस्तक्षेप नहीं किया। परन्तु इसी काल में सामाजिक सुधारकों का उदय हुआ जिन्होंने महिला अधिकारों और स्त्री उत्थान के लिए काम किया, जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी आदि।
महात्मा गांधी ने बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को समान अधिकार, शिक्षा, रोजगार के अवसर मिलने लगे, लेकिन समानता के लिए संघर्ष जारी रहा।
निष्कर्ष
प्राचीन काल में महिलाएं सम्मानित और स्वतंत्र थीं, परन्तु संपत्ति और उत्तराधिकार के सवालों के कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्थापित हुई, जिसने महिलाओं के अधिकारों को सीमित किया। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, जो कालक्रम में बिगड़ी। मध्यकालीन और अंग्रेजों के काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति और दयनीय हुई, फिर भी सुधार की कोशिशें हुईं। आज भी लैंगिक समानता पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु शिक्षा, कानून, जागरूकता और सामाजिक सुधारों के माध्यम से इसे प्राप्त करने की दिशा में प्रयास निरंतर जारी हैं।