कानून व विधि में जेंडर संबंधी भूमिका
देश में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए कई कानून बने हैं, जैसे कि सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम (1829), विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856), बाल विवाह निषेध अधिनियम (1929), दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961), मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार) अधिनियम (1986), घरेलू हिंसा रोधी कानून (2005), और यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून (2013) आदि। ये कानून महिलाओं के उत्पीड़न, हिंसा और भेदभाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
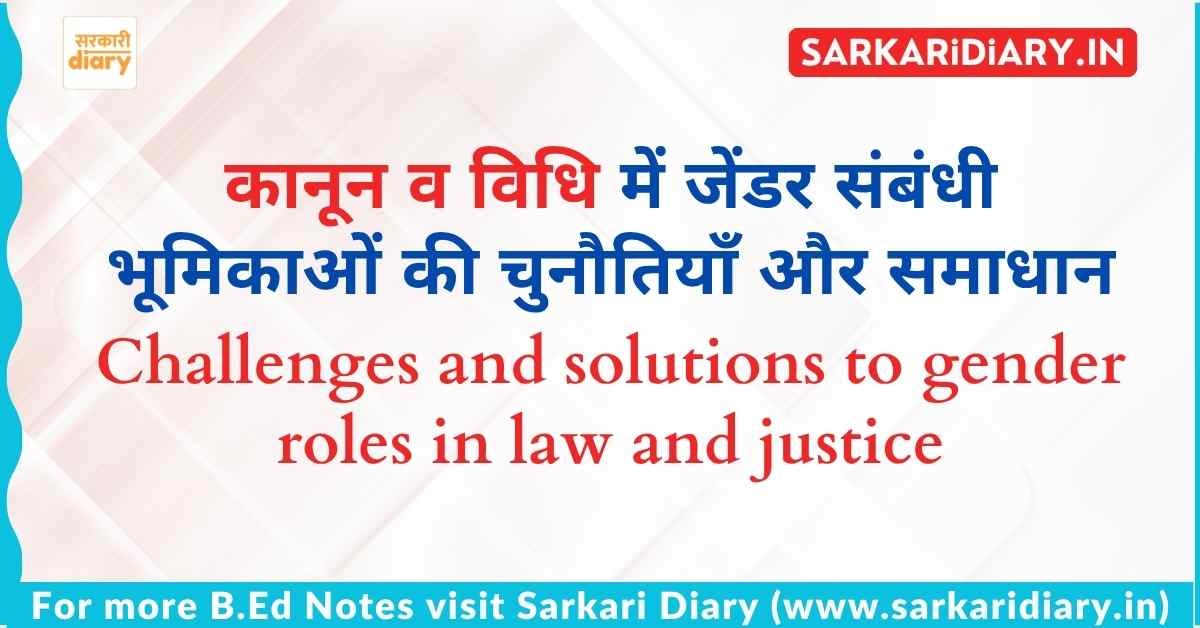
फिर भी, जेंडर संबंधी कई चुनौतियाँ कानून व्यवस्था में बरकरार हैं। उदाहरण के लिए, कुछ कानून अभी भी पूरी तरह प्रभावी नहीं हैं क्योंकि सजा के प्रावधान कम कड़े हैं, जिसके कारण अपराधों में कमी नहीं दिखती। जैसे, आईपीसी की धारा 509 में महिलाओं के अपमान के लिए एक साल की सजा का प्रावधान है जो नाकाफी माना जाता है। इसी तरह, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले भी बढ़ रहे हैं और इनके लिए कड़े कानून और त्वरित कार्रवाई की जरूरत है।
कानूनों के कार्यान्वयन में भी बड़ी समस्याएं हैं। न्यायालयों में लंबी प्रक्रियाओं से पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलने में बहुत समय लगता है। इसके अलावा, पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता और कभी-कभी उसमें लापरवाही या दमनकारी व्यवहार, महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने में बड़ी बाधा बनती है। यहां तक कि कुछ मामलों में पुलिस द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाएं भी सामने आई हैं, जो अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है।
समाधान के उपाय
कानूनों में संशोधन और सख्ती:
पुरानी और अधूरी कानून व्यवस्था को समय-समय पर संशोधित कर कठोर दंड निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि अपराधियों को कड़ी सजा मिल सके और अपराधों में कमी आए।
त्वरित न्याय और प्रभावी प्रवर्तन:
न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज करना आवश्यक है ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके। साथ ही, पुलिस और अन्य प्रशासनिक निकायों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने और कड़ी कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
न्यायालय और पुलिस प्रणाली में सुधार:
पुलिस में महिलाओं के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाना, शिकायत निस्तारण के लिए महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाना और यौन अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करना जरूरी है।
जागरूकता अभियान:
कानूनों के बारे में आम जनता और विशेषकर महिलाओं को जागरूक करना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और उनका सम्मान हो।
सर्वसमावेशी कानून:
नए कानून बनाते समय उन सभी वर्गों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कार्यस्थल की महिलाओं से लेकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं तक, ताकि कोई भी छूट न जाए।
सख्त निगरानी और जवाबदेही:
कानून लागू करने वाले अधिकारियों पर निगरानी रखनी चाहिए और यदि कोई लापरवाही करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो।
निष्कर्ष
एक सशक्त और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए कानूनों का होना और उनका सही तरीके से पालन अत्यंत आवश्यक है। जब तक कानून प्रभावी नहीं होंगे और प्रशासनिक तंत्र संवेदनशील नहीं बनेगा, तब तक जेंडर आधारित असमानता और उत्पीड़न पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए, कानूनों में सुधार के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता और प्रशासनिक सुधार भी जरूरी हैं ताकि सभी के लिए समानता और सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।





