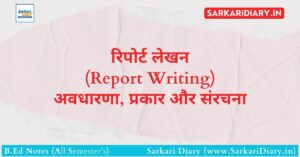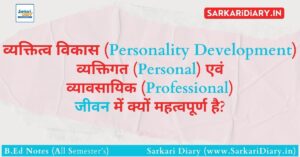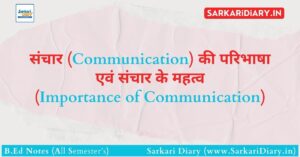परिवार एक छोटी सामाजिक संस्था है, जिसमें माता-पिता और संतान शामिल होते हैं। परिवार प्रेम के आधार पर एकजुट रहता है, लेकिन परिवार के सदस्यों की भूमिकाएँ और उनकी सोच जेंडर आधारित असमानताओं और समस्याओं को जन्म देती हैं। कुछ प्रमुख जेंडर संबंधी चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:
- बालिका और स्त्री की स्थिति व सम्मान में कमी
- घरेलू हिंसा
- भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याएँ
- असमान कार्य विभाजन
- लैंगिक पक्षपात और असमानता
कुछ परिवारों में लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। भारत में लड़कों को परिवार की उज्ज्वलता, बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, जबकि लड़कियों को ‘पराया धन’ समझा जाता है। कई बार लड़कियों का जन्म ही परिवार के लिए बोझ माना जाता है, जिसके कारण भ्रूण परीक्षण कर बालिका भ्रूण हत्या जैसी घटनाएँ होती हैं। पुत्री के जन्म के साथ ही दहेज की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, जो दहेज उत्पीड़न और यहां तक कि दहेज हत्या तक भी पहुंचती है।
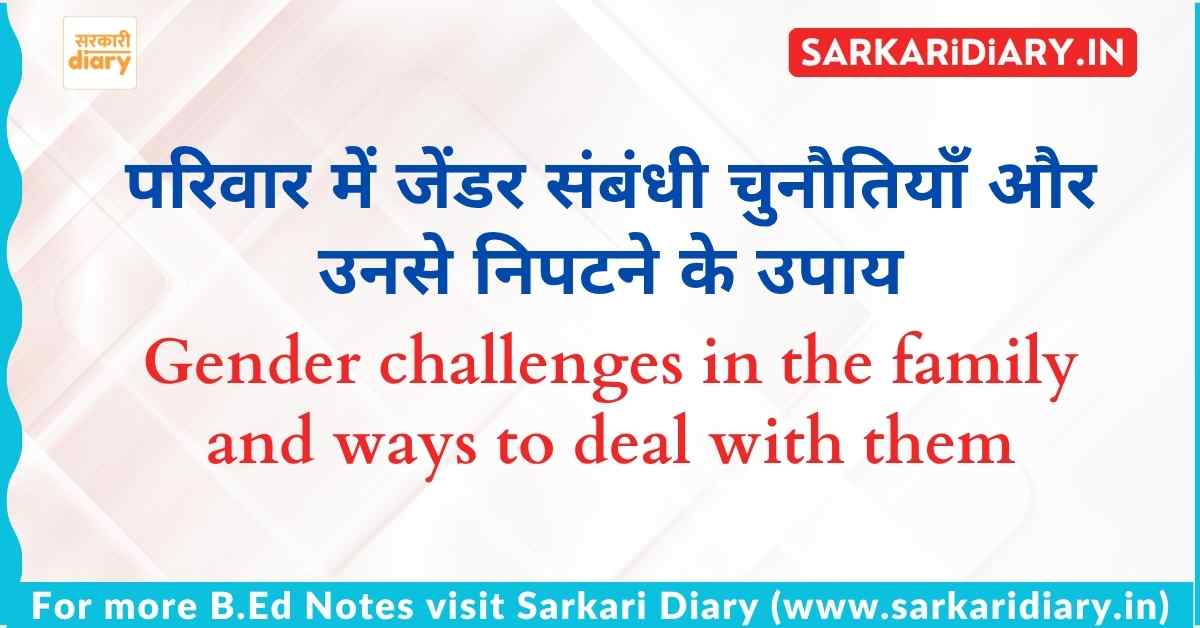
माता-पिता की सोच के कारण लड़कियों के पालन-पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य में भेदभाव होता है। लड़कों को मिलने वाली सुविधाओं से लड़कियाँ वंचित रह जाती हैं। लड़के आमतौर पर घरेलू कामों से दूर रहते हैं, जबकि घर के काम जैसे खाना बनाना, सफाई, बच्चों की देखभाल, पशु पालन आदि लड़कियों पर ही अधिक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई लड़कियाँ घर के कार्यों और कृषि में व्यस्त रहने के कारण नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पातीं। कम उम्र में सगाई और विवाह की वजह से भी कई लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं।
परिवारों में स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा एक सामान्य समस्या है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न शामिल है। घरेलू हिंसा के अधिकतर मामले छिपे रहते हैं और महिलाएं चुपचाप सहन करती हैं। महिलाओं की आत्महत्या भी जेंडर आधारित उत्पीड़न का एक दुखद परिणाम है। बालिका भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, लड़कियों के स्वतंत्र आवागमन पर रोक, घरेलू कार्यों का अत्यधिक दबाव, पालन-पोषण में भेदभाव, और शिक्षा एवं स्वास्थ्य में असमानता जैसी समस्याएँ पारिवारिक स्तर पर जेंडर संबंधी गंभीर चुनौतियाँ हैं।
इन चुनौतियों से निपटने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ-साथ उनके रिश्तेदारों और पड़ोसियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा जन जागरूकता अभियानों, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि के खिलाफ प्रदर्शन और कानूनी सहायता प्रभावी हो सकती है। घरेलू हिंसा के मामले महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत पुलिस में दर्ज कराए जा सकते हैं, जिसमें एनजीओ भी मदद करते हैं।
कुछ परिवारों में बालिकाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाएँ भी सुनने को मिलती हैं। ऐसी आशंका होने पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। स्कूलों में लड़कियों को आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) के प्रशिक्षण देना भी आवश्यक है।
सारांशतः, महिला सशक्तिकरण का पहला कदम परिवार से ही शुरू होना चाहिए। जेंडर आधारित भूमिकाओं और असमानताओं से निपटना परिवार से ही संभव है। शासन-प्रशासन द्वारा समय पर कानूनी कार्रवाई और नियमों का पालन कराए जाने से इन पारिवारिक समस्याओं को कम किया जा सकता है।